श्रीगणेश भारतीय जनमानस के सबसे अग्रणी और सर्वमान्य देवता हैं. देवता भी ऐसे जिनकी मान्यता रक्षक रूप में हैं और इस बात को बल मिलता है कि रामचरित मानस के रचनाकार संत तुलसीदास के एक वाकये से. घटनाक्रम ऐसा है कि रामभक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए बाबा तुलसी ने श्रीराम के कार्य में कोई विघ्न ने पड़े इसलिए विघ्नहर्ता को पुकारा था.
उन्होंने श्रीराम से पहले गणेश वंदना की और इसमें भी दिलचस्प है कि उन्होंने ये वंदना हनुमानजी की सलाह पर की थी. वही हनुमान जी जो खुद कलियुग में लोक रक्षक देवता हैं, लेकिन उन्होंने तुलसीदास से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए कहा तो सलाह दी कि पहले गणेश वंदना करो.
तुलसी दास के साथ हो रही थीं अप्रिय घटनाएं
घटनाक्रम ऐसा है कि अपने प्रभु श्रीराम की भक्ति में संत तुलसीदास ने मानस की रचना करने का संकल्प कर लिया था. अपने इस प्रयोजन और मन के काम की वह जब भी कभी शुरुआत करते थे तो कोई न कोई अड़चन आने लगती थी. वह काशी में अपनी कुटिया में मानस की पंक्तियां लिखना शुरू करते थे तो कभी चोर उन्हें चुरा ले जाए, कभी आग लग जाए.
कभी उन्हें कोई और कष्ट होने लगे. कहते हैं कि कलियुग ही उन्हें तरह-तरह से त्रास देकर सता रहे थे. हनुमान जी उनकी रक्षा तो कर ले रहे थे, लेकिन भक्त तुलसी दास का मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहा था. तब एक दिन हनुमान जी ने ही उन्हें सुझाव दिया कि आप श्रीराम से ही रक्षा करने की पुकार कीजिए. उनसे कहिए कि वह आपको हर तरह से निर्भय कर दें.
संत तुलसी ने रची गणेश वंदना
तब तुलसीदास ने रामचरित मानस से पहले विनय पत्रिका की रचना शुरू की और इसमें भी हनुमान जी की सलाह पर सबसे पहले गणेश वंदना की. संत तुलसी दास की गणेश वंदना इतनी प्रभावशाली थी कि खुद महागणपति को रामचरित मानस के निर्विघ्न पूर्ण होने का आश्वासन दिया. इस कथा को विस्तार से बताते हुए आचार्य हिमांशु उपमन्यु ( संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) कहते हैं कि बाबा तुलसी ने गणेश वंदना के लिए विशेष पद लिखा, उसे दिन के सबसे पहले प्रहर (सुबह) में गाया और उन्होंने इसके शास्त्रीय पक्ष का इतना अधिक ध्यान रखा कि उन्होंने इस आधार पर एक-एक शब्द और मात्रा चुनकर इस तरह छंद बद्ध की, ताकि इसे दिन के पहले प्रहर के राग में गाया जा सके.
राग बिलावल में रची गई गणेश वंदना
दिन के पहले प्रहर का राग है, राग बिलावल. तो श्रीगणेश ने विनय पत्रिका में दर्ज अपनी इस पहली रचना को राग बिलावल से आबद्ध (सजाया) किया है. यह गणेश वंदना बहुत प्रसिद्ध हुई और आज भी इसे राग बिलावल में ही गाया जाता है.
गाइये गनपति जगबंदन,
संकर-सुवन भवानी-नंदन॥
सिद्धि-सदन गज-बदन बिनायक,
कृपा-सिंधु सुंदर सब-लायक॥
मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता,
बिद्या-बारिधि, बुद्धि-बिधाता॥
मांगत तुलसिदास कर जोरे,
बसहिं रामसिय मानस मोरे॥
(संपूर्ण जगत् के वंदनीय, गुणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए, जो शिव-पार्वती के पुत्र और उनको प्रसन्न करने वाले हैं. जो सिद्धियों के स्थान हैं, जिनका हाथी का-सा मुख है, जो समस्त विघ्नों के नायक हैं यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सुंदर है, सब प्रकार से योग्य हैं. जिन्हें लड्डू बहुत प्रिय है, जो आनंद और कल्याण को देने वाले हैं, विद्या के अथाह सागर हैं, बुद्धि के विधाता हैं. श्री गणेश से यह तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगता है कि मन मंदिर में श्री सीता राम जी सदा निवास करें.)
विनय पत्रिका में शामिल है गणेश वंदना
इस तरह प्रथम पूज्य की प्रथम वंदना के लिए प्रथम प्रहर का समय चुनते हुए प्रथम प्रहर के प्रथम राग का भी चिंतन करके संत तुलसीदास ने प्रथमेश (श्रीगणेश) की भक्ति को सार्थक किया फिर विनय पत्रिका की रचना संपूर्ण हुई. इसे पूरा करके संत तुलसी ने इसे श्रीराम के चरणों में अर्पित कर दिया और रक्षा की मांग की. विनय पत्रिका के विनम्र और भावभीने पदों का ऐसा असर हुआ कि श्रीराम ने खुद इस पर हस्ताक्षर किए और अपने भक्त तुलसीदास को हर भय से निर्भय कर दिया.
कहते हैं कि, जब इस स्तुति को हृदय से गाया जाता है, तो एक अद्भुत अनुभूति होती है. एक आंतरिक प्रकाश, एक शांति, एक चेतना का उदय हो जाता है. यह स्तुति फिर केवल पाठ नहीं रहती यह एक सेतु बन जाती है जो भक्त और भगवान को जोड़ देती है.
राग बिलावल का परिचय
भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग बिलावल सातों शुद्ध स्वरों के प्रयोग के चलते शुद्ध राग, प्राकृतिक राग भी कहलाता है. हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि राग बिलावल में आरोह में मध्यम स्वर वर्जित है, जबकि अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है. इसकी उत्पत्ति बिलावल थाट से मानी जाती है. बिलावल राग का वादी स्वर धैवत (ध) और सम्वादी स्वर गंधार (ग) है. राग की जाति सम्पूर्ण – सम्पूर्ण है, और इसका गायन समय प्रातःकाल होता है. कहते हैं कि इसकी उत्तपत्ति गुजरात के वेरावल से हुई है, लेकिन कई विद्वान इसे कर्नाटक संगीत की विधा से निकला राग बताते हैं.
इस गाने में जब गायक आरोह लेता है तो आपको मध्यम स्वर का लोप साफ-साफ पता चलता है, लेकिन अवरोह में सातों स्वर जीवंत हो उठते हैं. भातखंडे ने दस थाट के अंतर्गत सभी रागों का वर्गीकरण किया है. कम से कम सात स्वरों के प्रयोग से थाट का निर्माण होता है. थाट के स्वरों के आधार पर ही रागों की रचना की जाती है.
---- समाप्त ----

.png) 1 week ago
1
1 week ago
1





















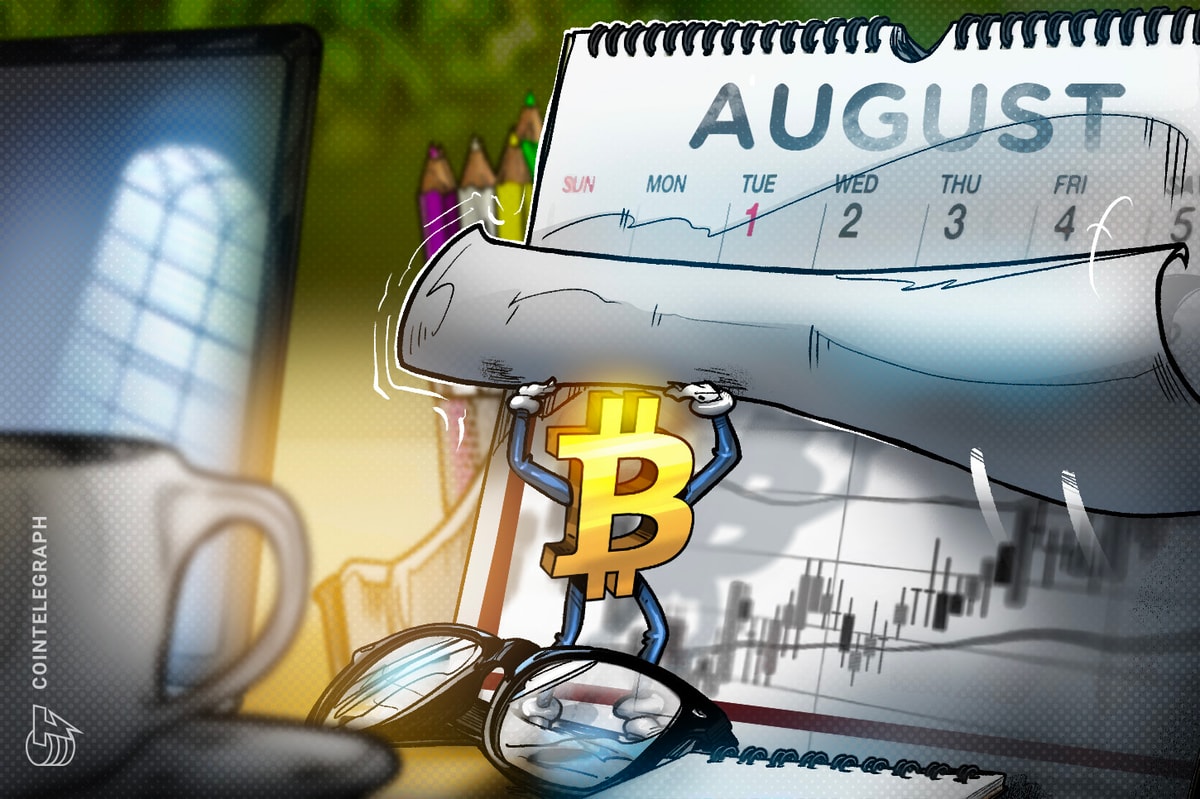
 English (US) ·
English (US) ·