मुस्कुराते मोदी, मुट्ठी बांधे पुतिन, गर्मजोशी से हाथ मिलाते शी जिनपिंग... चीन के SCO मीटिंग से आई तीन महाशक्तियों की ये तस्वीरें ग्लोबल पॉलिटिक्स के रिअलाइनमेंट की कहानी कहती हैं. लेकिन तस्वीरों के सिम्बॉलिज्म में सच्ची और गहरी दोस्ती की भावना कितनी है? दोस्ती में गर्मजोशी का ये दौर कितना लंबा चलेगा? क्या वाकई ये नई दोस्ती की शुरुआत हुई है अथवा इस एकजुटता की वजह ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियां हैं जिसने भारत, चीन और रूस को एक दूसरे को संभालने के लिए साथ आने पर मजबूर किया है.
अगर भविष्य में अमेरिका टैरिफ को लेकर अपनी नीतियों में लचीलापन लाता है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील सील हो जाता है तो तीन महाशक्तियों की ये दोस्ती क्या इसी तरह से परवान चढ़ती रहेगी. या भारत को फिर से डिप्लोमेसी का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा. आइए समझते हैं.
तस्वीरें रिश्तों में गर्मजोशी और उम्मीद बेचती हैं, लेकिन इन्हें टिकाऊ तभी माना जा सकता है जब दोस्ती के प्रति कमिटमेंट हो. क्या चीन के साथ भारत के ऐतिहासिक अविश्वास के अनुभवों को देखते हुए चीन से आई गर्मजोशी की इन तस्वीरों पर यकीन किया जा सकता है.
भारत-चीन रिश्ते दशकों से सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक असहमति से जूझते आए हैं. डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों विशेष रूप से भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए 50% टैरिफ (25% सामान्य + 25% दंडात्मक) ने भारत को चीन के करीब ला दिया है.
दक्षिण एशिया में कहां-कहां और कैसे टकराते हैं भारत-चीन के हित
लेकिन भारत-चीन के बीच सीमा विवाद को छोड़ भी दें तो एशिया महादेश में भारत और चीन के बीच टकराव की कई वजहें हैं. दक्षिण एशिया के कई देशों में भारत का चीन से आर्थिक टकराव है. पिछले कुछ सालों में चीन ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में अपने प्रभाव क्षेत्र (Sphere of influence) को खूब बढ़ाया है. चीन जब इन क्षेत्रों में आर्थिक विस्तार और कर्ज नीति के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा तब भारत-चीन की इस दोस्ती की असली परीक्षा होगी. क्योंकि इन सभी देशों में चीन के दबदबे का अर्थ है भारत के प्रभुत्व में कमी. ऐसी किसी स्थिति में भारत क्या करेगा? भारत के पड़ोसी देशों में चीन का हैवी 'आर्थिक' निवेश है.
नेपाल भारत का सबसे नजदीकी पड़ोसी है. दोनों देशों के बीच सदियों से सांस्कृतिक संबंध है. लेकिन आर्थिक विस्तारवाद की पॉलिसी पर चल रहा चीन सालों से नेपाल पर प्रभाव बढ़ा रहा है. चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट्स के जरिये नेपाल में निवेश कर रहा है. साथ ही चीन ट्रांस-हिमालयन रेल परियजोना के जरिये भी नेपाल तक अपनी पहुंच आसान करना चाहता है. जो भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है.
श्रीलंका में चीन हंबनटोटा बंदरगाह पर नियंत्रण चाहता है, वही भारत का सबसे नजदीकी पड़ोसी होने के नाते नई दिल्ली की मंशा है कि श्रीलंका उसके प्रभाव क्षेत्र में रहे. भारत ने भी कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है. दोनों देश समुद्री प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं. चीन कई बार अपने समुद्री पोत को इस इलाके में भारत पर निगहबानी के लिए भेजता रहता है.
मालदीव एक ऐसा देश है जहां चीन और भारत के निवेश हितों का सीधा टकराव है. चीन ने मालदीव में करोड़ों ड़ॉलर का निवेश किया है. इस प्रक्रिया में भारतीय कंपनियों को यहां कई प्रोजेक्ट खोने पड़े हैं. मालदीव की पिछली सरकारें जबर्दस्त रूप से चीन के प्रभाव में थी.
बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. यहां के कर्ता-धर्ता मोहम्मद युनूस ने कुछ ही दिन पहले चीन का दौरा किया था और भारी भरकम निवेश के लिए हाथ फैलाया था.
रणनीतिक रूप से चीन बांग्लादेश में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जैसे पायरा पोर्ट और ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. इससे भारत की सुरक्षा का मसला खड़ा हो गया है. सवाल पूर्वोत्तर राज्यों तक चीन के पहुंच का भी है. वहीं चीन का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान-बांग्लादेश के रिश्तों को भी आगे बढ़ाता है, इससे भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है. आर्थिक रूप से भी चीन का कर्ज बांग्लादेश को उसकी ओर झुका रहा है.
इन उदाहरणों से सवाल उठता है कि दक्षिण एशिया में जब हाथी और ड्रैगन की महात्वाकांक्षाएं टकराएंगी तो फिर भारत को सतर्क रहना होगा. इससे आगे बढ़ते हैं और बात म्यांमार की.
म्यांमार में भारत और चीन के हित आमने-सामने हैं. चीन वहां बड़े पैमाने पर खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और बंदरगाह निर्माण कर रहा है ताकि अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना को आगे बढ़ा सके, जबकि भारत कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट परियोजना को बढ़ाना चाहता है. म्यांमार के आस-पास भारत की मौजूद सामरिक स्थिरता, पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है. चीन म्यांमार की सेना और जातीय विद्रोही गुटों को आर्थिक-कूटनीतिक समर्थन देकर अपने हित साधता है. इससे भी दोनों मुल्कों के बीच टकराव पैदा होता है.
भूटान के डोकलाम क्षेत्र में भारत की सुरक्षा चिंताएं और चीन की सड़क निर्माण गतिविधियां भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण हैं.
आयरन ब्रदर्स की दोस्तियां और भारत की चिंताएं
इन सब के बीच पाकिस्तान का फैक्टर सबसे बड़ा है, जहां अपनी लगभग समानांतर सत्ता चलाता है. 'आयरन ब्रदर' की दोस्ती की आड़ में चीन पाकिस्तान को पैसा, डिफेंस तकनीक, स्पेस तकनीक और न जाने क्या क्या दे रहा है. इसके एवज में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चीन को हर तरह की आजादी दे दी है. CPEC इसका उदाहरण है. चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है. यहां चीन द्वारा किसी भी तरह का निर्माण दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर ले जाएगा.
दक्षिण एशिया में चीन के विस्तारवाद का क्या होगा?
भारत और चीन ने साझेदारी, सहयोग और शांति की बातों से अपने रिश्तों को मजबूत करने की मंशा जरूर जाहिर की है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इन समीकरणों की नींव सामरिक और आर्थिक हितों में छिपी है. जब तक सीमा विवाद शांत हैं, व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ता है, और घरेलू राजनीति में रिश्तों को समर्थन मिलता है- दोस्ती आगे बढ़ सकती है. लेकिन जैसे ही चीन दक्षिण एशिया में विस्तारवाद की नीति पर बढ़ना शुरू करेगा, जिसके लिए कई फ्रंट खुले हुए हैं, तो भारत-चीन के रिश्तों में पुरानी ठंडक वापस आ सकती है.
रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने एक्स पर लिखा है कि पीएम मोदी और जिनपिंग की मीटिंग को लेकर मीडिया हाइप के बावजूद इस मुलाकात से ठोस निष्कर्ष कम निकले और आप्टिक्स ज्यादा पैदा हुआ. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विवाद के जो कोर मुद्दे हैं जैसे सुरक्षा, सीमा विवाद और ट्रेड पर कुछ खास प्रगति नहीं देखने को मिली.
ब्रह्म चेलानी ने इस मुद्दे पर एक लेख में लिखा है कि, 'तुष्टिकरण ने दुनिया को अपने ढंग से चलाने की इच्छा रखने वाली शक्तियों को कभी काबू में नहीं किया है, बल्कि अक्सर उन्हें और मज़बूत किया है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में अपने शुरुआती वर्षों में यह कठिन अनुभव किया, जब चीन ने हिमालय क्षेत्र की यथास्थिति को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश के लिए उनकी सद्भावना का फायदा उठाया, लेकिन अब पीएम मोदी के एक बार फिर से उसी जाल में फंसने का खतरा है.'
भारत के सामने बड़ा प्रश्न यह है कि अगर भविष्य में इंडिया को टैरिफ पर अमेरिका से रियायत मिलती है तो भारत को अपनी सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक नीतियों का संतुलन फिर से बदलना होगा. गौरतलब है कि अमेरिका की नीतियों में आया बदलाव ट्रंप केंद्रित है. ट्रंप की पहली पारी भी भारत के लिए मुश्किलें लेकर नहीं आई थी. घरेलू मजबूरियों, यूएस इकोनॉमी पर दबाव और MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) जैसी नीतियों की वजह से दूसरी पारी में ट्रंप ने आक्रामक विदेश और व्यापार नीति पर चलना शूरू किया है. नहीं तो 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के रिश्ते सहयोग भरे ही रहे हैं. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है.
हालांकि अभी तक अमेरिका ने अभी अपनी टैरिफ नीतियों में बदलाव का कोई भी संकेत नहीं दिया है. राष्ट्र्पति ट्रंप ने अपनी ओर से एकतरफा दावा जरूर किया है कि भारत अपने टैरिफ को घटाने को तैयार है. अमेरिका के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भी कहा है कि भारत जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन की तरह अमेरिका से टैरिफ घटाने पर कोई बात नहीं कर रहा है. हालांकि भारत ने इन बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
---- समाप्त ----

.png) 6 days ago
1
6 days ago
1





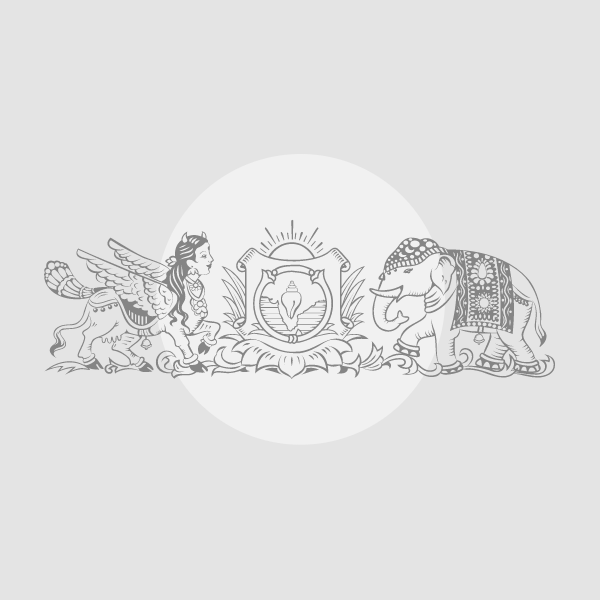
















 English (US) ·
English (US) ·