भारत पिछले 10 सालों में बाढ़ का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. 2014 से 2024 के बीच देश के 3 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र. यानी देश की कुल जमीन का 10%, किसी न किसी तरह की बाढ़ से प्रभावित हुआ. खासकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मॉनसून की भारी बारिश ने तबाही मचाई. नदियों का उफान, कमजोर बांध और जल निकासी की रुकावट ने बाढ़ को और भयानक बना दिया.
2025 में पंजाब की बाढ़ ने स्थिति को और गंभीर कर दिया. सतलज, ब्यास और रावी नदियों में उफान और भाखड़ा, पोंग व रणजीत सागर बांधों से पानी छोड़े जाने से 1902 गांव डूब गए. 3.84 लाख लोग प्रभावित हुए और 1.7 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गईं. गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. क्लाइमेट चेंज से भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसने इस आपदा को और बढ़ाया.
यह भी पढ़ें: लगभग हर दिन आपदा का सामना कर रहा हिमालय... बढ़ता जा रहा बर्बादी का सिलसिला
इन बाढ़ों के पीछे प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं. भारी बारिश के साथ-साथ नदियों के किनारों पर बस्तियां और खेती, कमजोर बांध और नहरों में गाद जमा होना बड़ा कारण रहा है. शहरी क्षेत्रों में पुरानी ड्रेनेज सिस्टम भी बाढ़ का कारण बनी. भविष्य में बाढ़ से बचने के लिए मजबूत बांध, नदियों की सफाई, अतिक्रमण रोकना और बेहतर चेतावनी सिस्टम जरूरी हैं.

पंजाब अन्न के भंडार से पानी के 'कटोरे' में तब्दील
पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है. इस साल भयंकर बाढ़ की चपेट में है. अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश, कमजोर बांध, नदियों के किनारों पर अतिक्रमण और प्राकृतिक जल निकासी की रुकावट ने इस आपदा को और भयावह बना दिया.
यह बाढ़ पिछले तीन दशकों में सबसे विनाशकारी मानी जा रही है जिसने 1902 गांवों को डुबो दिया. 3.84 लाख लोगों को प्रभावित किया. 1.7 लाख हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर दिया. पंजाब में हर साल मॉनसून के दौरान बाढ़ आती है, लेकिन 2025 की बाढ़ ने 1988 के बाद सबसे ज्यादा तबाही मचाई.
यह भी पढ़ें: नदी में कॉलोनियां या कॉलोनी में नदी? दिल्ली में यमुना की बाढ़ की जिम्मेदारी किसकी, कैसे थमेगी हर साल की तबाही
नदियां खतरनाक जलस्तर तक बढ़ी
सतलज, ब्यास और रावी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया. वजह थी हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश. भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांधों से पानी छोड़ा गया, इससे निचले इलाके डूब गए. पंजाब के मैदानी इलाकों में पानी भरने लगा. फैलने लगा.

गुरदासपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 324 गांव डूबे. 1.45 लाख लोग प्रभावित हुए. फिर अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, पठानकोट, कपूरथला, होशियारपुर, तरनतारन और पटियाला भी बुरी तरह प्रभावित हुए. 5 सितंबर तक 43 लोगों की मौत हो चुकी थी. 1.7 लाख हेक्टेयर फसलें, खासकर धान बर्बाद हो गईं. पंजाब के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया.
शहरों में भी हालत खराब थी. मोहाली, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और चंडीगढ़ में 1-3 सितंबर को भारी बारिश से सड़कें, घर और दुकानें डूब गईं. यह शहरी फ्लैश फ्लड का नया रूप था, जो पुरानी सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी को दिखाता है.
बाढ़ के कारण: प्रकृति और इंसानी लापरवाही
पंजाब की बाढ़ के पीछे प्रकृति और इंसानी गलतियों का कॉम्बीनेशन है. आइए, इसे समझते हैं...
यह भी पढ़ें: 6% अधिक बारिश से पूरा देश बेहाल...हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में मॉनसून ने बरसाया कहर
प्राकृतिक कारण
- भारी बारिश: मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब में 30 अगस्त तक 443 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 357.1 मिमी से 24% ज्यादा थी. 28 अगस्त से 3 सितंबर तक 48% अतिरिक्त बारिश हुई. हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से नदियों में अचानक पानी बढ़ गया.
- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन ने बारिश को और तीव्र कर दिया. मॉनसून ट्रफ, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती सिस्टम ने बारिश को बढ़ाया.
- बांधों से पानी: भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांधों में पानी की अधिकता के कारण लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसने बाढ़ को और बिगाड़ दिया.

इंसानी गलतियां
- कमजोर बांध (धूंसी बांध): सतलज, ब्यास और रावी नदियों के किनारे बने अस्थाई बांध (धूंसी बांध) कमजोर थे. इनकी मरम्मत और मजबूती के लिए पहले से काम नहीं हुआ.
- नदियों के किनारों पर अतिक्रमण: नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में खेती और बस्तियां बस गईं. रूपनगर के सतलज में 'बेला बेल्ट' पर 50000 लोग और गुरदासपुर में ब्यास-रावी के बाढ़ क्षेत्रों में 450 गांव हैं.
- सिल्ट जमा होना: नदियों और बांधों में गाद (सिल्ट) जमा होने से उनकी पानी ले जाने की क्षमता कम हो गई. डी-सिल्टेशन का काम समय पर नहीं हुआ.
- बंद नाले और नहरें: दक्षिण-पश्चिम पंजाब में नहरों का जाल है, लेकिन सड़कें, पुल और कंक्रीट की दीवारों ने प्राकृतिक नालों को बंद कर दिया, जिससे शहरी बाढ़ बढ़ी.
- खराब प्रबंधन: जिला बाढ़ प्रबंधन योजनाएं थीं, लेकिन उनका लागू होना देर से और सीमित रहा. बांधों से पानी छोड़ने की योजना और चेतावनी में कमी थी.
यह भी पढ़ें: इस बार बारिश ज्यादा हो रही या मौसम के 'सरप्राइज' से मच रही इतनी तबाही? कश्मीर से पंजाब-दिल्ली तक बाढ़ का कहर
नुकसान
- कृषि: 1.7 लाख हेक्टेयर फसलें, खासकर धान बर्बाद. पंजाब भारत का 20% गेहूं और 12% चावल पैदा करता है, उस उत्पादन को बड़ा आर्थिक झटका लगा.
- मानव और पशु हानि: 43 लोगों की मौत. कई लापता. पशुधन बह गया. कुछ पशु छतों पर फंसे.
- संपत्ति और बुनियादी ढांचा: घर, सड़कें और बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान. गुरदासपुर में 1.45 लाख लोग और 324 गांव प्रभावित.
- शहरी बाढ़: लुधियाना, जालंधर और मोहाली में सड़कें और कॉलोनियां डूब गईं.
- आर्थिक नुकसान: शुरुआती अनुमान 1700-2000 करोड़ रुपये का नुकसान. बाद में 1,219 करोड़ रुपये बताया गया.
केंद्र और राज्य का टकराव
केंद्रीय जल आयोग (CWC) की रिपोर्ट्स में कहा गया कि पंजाब की नदियां ऐतिहासिक जलस्तर तक नहीं पहुंचीं, बल्कि मॉनसूनी बाढ़ की स्थिति थी. लेकिन स्थानीय पत्रकारों और मीडिया ने बताया कि 14 अगस्त से बाढ़ शुरू हो गई थी. 25 से यह विनाशकारी हो गई. सरकार को 10 दिन पहले चेतावनी थी, लेकिन कार्रवाई देर से हुई.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपये की मदद मांगी, लेकिन केंद्र ने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पहले से पैसे हैं. विपक्षी दलों ने AAP सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया.
भविष्य के लिए उपाय
बाढ़ से बचने के लिए विशेषज्ञों ने ये सुझाव दिए हैं...
- बाढ़ क्षेत्रों पर नियंत्रण: नदियों के किनारों पर खेती और बस्तियां रोकने के लिए सख्त नियम लागू करें.
- विभागों का सहयोग: IMD, सिंचाई विभाग और BBMB मिलकर योजना बनाएं, कमजोर इलाकों की मैपिंग करें, और जल्दी चेतावनी दें.
- बांधों की मजबूती: धूंसी बांधों को मजबूत करें, मॉनसून से पहले डी-सिल्टेशन करें.
- शहरी ड्रेनेज: पुरानी सीवरेज और स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम को अपग्रेड करें.
- फंडिंग: नहरों और नालों की सफाई के लिए पर्याप्त पैसा दें.
- समुदाय की भागीदारी: स्थानीय लोग और NGO को तैयारियों और राहत कार्यों में शामिल करें.
- जल्द मुआवजा: बाढ़ के बाद नुकसान की भरपाई और बीमारियों से बचाव के लिए तुरंत मदद दें.
---- समाप्त ----

.png) 5 hours ago
1
5 hours ago
1



















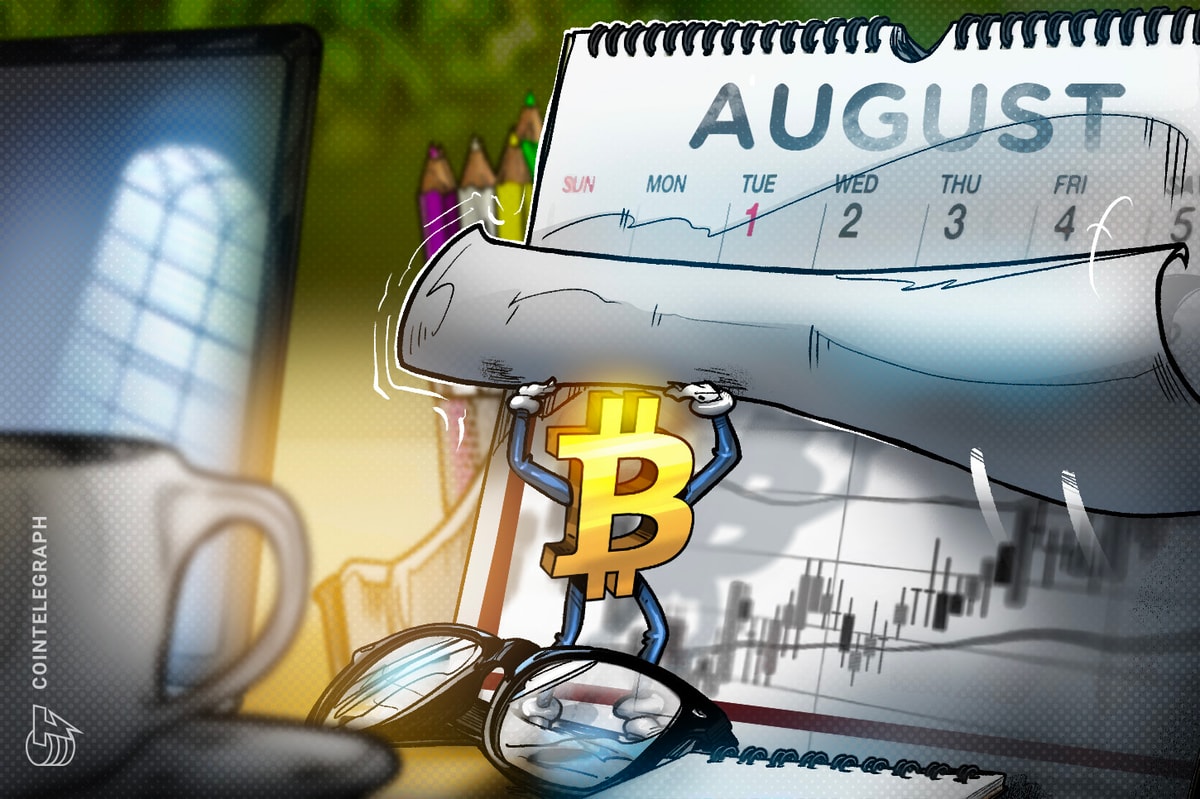

 English (US) ·
English (US) ·